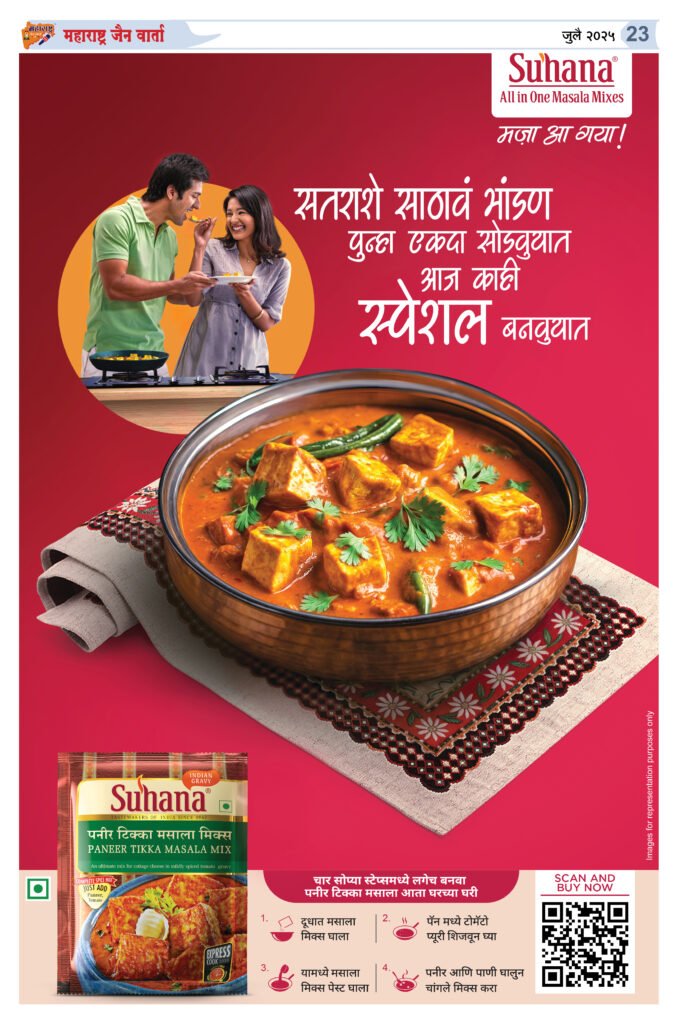महाराष्ट्र जैन वार्ता
पुणे : जब हम मनुष्य के रूप में जन्म लेते हैं, तब हमारे सामने जीवन के प्रति कोई न कोई लक्ष्य या उद्देश्य होना आवश्यक होता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उसे प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर होते हैं, वे निश्चित ही दूसरों से अलग और विशेष बनते हैं। जीवन के मार्ग पर चलते समय श्रद्धा का आधार आवश्यक होता है, ऐसा प्रतिपादन प. पू. प्रवीणऋषिजी म. सा. ने किया। वे परिवर्तन चातुर्मास 2025 के अंतर्गत आयोजित प्रवचन माला में संबोधित कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि हमारे लक्ष्य और संकल्प हमें इच्छित स्थल तक पहुँचने का मार्ग दिखाते हैं। लेकिन जिनके पास कोई उद्देश्य नहीं होता, उनके सामने भले ही अनेक रास्ते खुले हों, फिर भी वे कभी मंज़िल तक नहीं पहुँच सकते, क्योंकि उनके जीवन को कोई सही दिशा नहीं मिली होती।
इसीलिए बिना उद्देश्य के जीने वाला व्यक्ति एक भ्रमजाल में जी रहा होता है। इसलिए चलते समय सबसे पहले लक्ष्य की निश्चितता यह पहला सूत्र होना चाहिए। दूसरा सूत्र यह है कि हमारे चलने को श्रद्धा का आधार चाहिए।
यह श्रद्धा कैसी होनी चाहिए? यह श्रद्धा होनी चाहिए ज्ञान की, अपने चरित्र की और अपने द्वारा निश्चित किए गए उद्देश्य की। जब हम अज्ञान में, द्विधा की स्थिति में या संशय के साथ चलते हैं, तब हम अर्जुन जैसे हो जाते हैं। इसका सीधा अर्थ यह है कि हम अपने ही भीतर हार चुके होते हैं, भ्रमित हो चुके होते हैं।
इसलिए जब हम किसी दिशा में अग्रसर हो रहे होते हैं, तब हमें यह परखना चाहिए कि हमारे मन में कौन-से भाव उत्पन्न हो रहे हैं। क्या उनमें श्रद्धा, आस्था या भक्तिभाव जागृत है? इस बात का निरीक्षण करना आवश्यक है।
इसका उदाहरण देते हुए प. पू. प्रवीण ऋषिजी म. सा. ने कहा, जब हम माँ को केवल माँ के रूप में नहीं, बल्कि ईश्वर स्वरूप में देखते हैं, तब वह माँ हमारे लिए श्रद्धा का प्रतीक बन जाती है। ऐसा ही पिता, गुरु या घर के संबंध में भी कहा जा सकता है।
जब हम अपने घर को मात्र एक निवास नहीं, बल्कि एक मंदिर के रूप में देखते हैं, तब उसमें देवत्व का भाव जागृत होता है। और इसी श्रद्धा से तीर्थ की उत्पत्ति होती है। ‘तीर्थ’ केवल कोई स्थान नहीं होता, बल्कि वह जगह होती है जहाँ आपकी इच्छाएँ और सपने पूर्ण होते हैं।
जहाँ पापों का अंत होता है, वही तीर्थ होता है। जब हमारी वाणी से किसी को दुःख होता है और हमें इस बात की अनुभूति होती है, तब हमारे भीतर पाप-बोध उत्पन्न होता है। और जब यह बोध उत्पन्न होता है, तब हम उस पाप से मुक्ति के उपाय खोजना शुरू कर देते हैं। यही श्रद्धा की शुरुआत है, जो हमारे भीतर परिवर्तन का मार्ग खोलती है।
इसलिए प्रतिदिन की क्रियाओं में श्रद्धा का समावेश होना अत्यंत आवश्यक है। चाहे दिन हो या रात्रि, निद्रा की अवस्था हो या जागृत, हम अकेले हों या समूह में हमारे आत्मा का स्वभाव श्रद्धा ही हो, यह भाव मन में दृढ़ होना चाहिए।
परंतु यह करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। यदि श्रद्धा से ध्यान किया जा रहा है लेकिन व्यवहार संशयपूर्ण है, तो वह श्रद्धा वास्तविक नहीं मानी जा सकती। इसका अर्थ है कि वह केवल दिखावा है, अस्थायी है।
इसलिए श्रद्धा कैसी होनी चाहिए? वह शाश्वत होनी चाहिए। मोह, क्रोध, अहंकार और संशय ये क्षणिक होते हैं, परंतु श्रद्धा एक सतत, निर्मल जलप्रवाह के समान होती है। उसका अस्तित्व किसी एक समय या स्थान तक सीमित नहीं होता, वह सार्वकालिक और विश्वव्यापी होती है।
इसलिए जब भी जीवन में आगे बढ़ें, तो श्रद्धा और भक्ति के साथ चलें। आपसी संबंधों में श्रद्धा और भक्ति की डोर बनाएं। श्रद्धा करें और श्रद्धा का सम्मान करें। व्यक्ति से अधिक उसके भीतर विद्यमान भक्ति को पहचानें। श्रद्धा का अस्तित्व केवल श्रद्धा पर ही आधारित है, क्योंकि अंततः श्रद्धा ही जीवन का प्राण है।