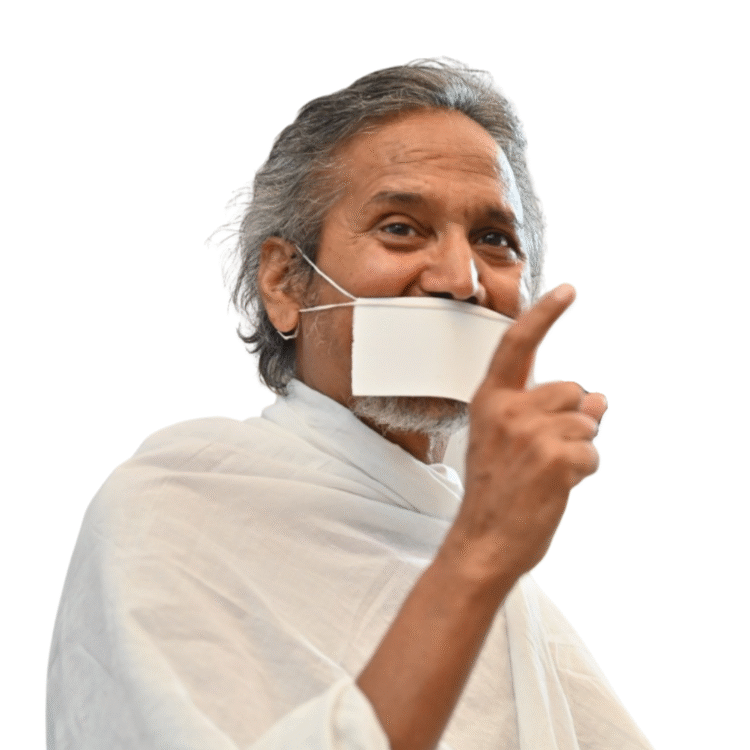महाराष्ट्र जैन वार्ता
पुणे : किसी व्यक्ति के पास सभी सुख-सुविधाएँ, समृद्धि, ऐशोआराम और वैभव हो सकता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वह भीतर से सचमुच सुखी है। सुख बाहरी वस्तुओं से प्राप्त होने के बजाय आपके अंतर्मन में होना चाहिए। सुख की परिभाषा जैसी परिस्थिति के अनुसार बदलती रहती है, वैसे ही सुख भी परिस्थितियों के साथ बदलता है।
इसलिए हमें सुखी होने से अधिक समर्थ बनने पर ध्यान देना चाहिए। वे माता-पिता जो सामर्थ्य का महत्व समझते हैं और उसी के अनुसार अपने बच्चों को गढ़ते हैं, वही सच्चे अर्थों में माता-पिता कहलाने के योग्य होते हैं।
बच्चों से प्रेम करके हम उन्हें सुखी बना सकते हैं, लेकिन समर्थ या सामर्थ्यवान नहीं बना सकते। यदि आप अपने बच्चों के सामने सभी सुख-सुविधाएँ परोस देंगे, तो उनकी प्रगति के मार्ग में सबसे बड़ा अवरोधक आप स्वयं होंगे।
क्योंकि आपने उन्हें जीवन के उतार-चढ़ाव, सफलता-असफलता का अनुभव करने का अवसर ही नहीं दिया। उन्हें श्रम का महत्व नहीं बताया। इसलिए यदि बच्चों को वास्तव में गढ़ना है और उनका सर्वांगीण विकास करना है, तो उन्हें समर्थ बनाना आवश्यक है।
स्वयं का परीक्षण करते समय आपको एक प्रश्न अवश्य पूछना चाहिए -“क्या मैं केवल सुखी बनना चाहता हूँ या समर्थ?” उसी के अनुसार अपने भीतर परिवर्तन लाना होगा। कभी-कभी कमज़ोर लोग समर्थ व्यक्ति के कंधे पर बंदूक रखकर अपने काम निकालते हैं।
ऐसे लोगों से दूर रहना ही उचित है। जो व्यक्ति स्वयं समर्थ होते हैं, वही दूसरों के सामर्थ्य को पहचानते हैं। इसी कारण जिस व्यक्ति के संग हम रहते हैं, वैसा ही हम बनते जाते हैं। इसलिए सामर्थ्यवान लोगों के सान्निध्य में रहना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि इसी समर्थता से वास्तविक सुख का जन्म होता है।
इसका अर्थ यह है कि – जो सुखी है, वह ज़रूरी नहीं कि समर्थ भी हो। लेकिन जो समर्थ है, वह कभी दुखी नहीं हो सकता। यही नियम ध्यान में रखते हुए यदि हम सुख की परिभाषा बदलें, तो हम अपने जीवन को सामर्थ्यवान बनाने की दिशा में निश्चित रूप से आगे बढ़ सकते हैं।